(विभूति नारायण ओझा -विभूति फीचर्स)
प्रस्तुति- सुरेश प्रसाद आजाद

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन का मूल है, ‘आत्मवत सर्वभूतेषु’. इसका मतलब है कि सभी में एक और एक में सभी को देखना. उनके इस दर्शन के बारे में ज़्यादा जानकारीः
- एकात्म मानववाद, मानव जीवन और पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र संबंध का दर्शन है.
- यह दर्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 22 से 25 अप्रैल, 1965 को मुंबई में चार व्याख्यानों के ज़रिए पेश किया था.
- एकात्म मानववाद को किसी वाद के रूप में नहीं, बल्कि एक दर्शन के रूप में देखा जाना चाहिए.
- एकात्म मानववाद के मुताबिक, व्यक्ति, परिवार, समाज, जाति, राष्ट्र, दुनिया, और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हैं.
- इस दर्शन के मुताबिक, सभी एक-दूसरे के पूरक हैं और एक-दूसरे का स्वाभाविक सहयोगी हैं.
- एकात्म मानववाद के मुताबिक, समाज व्यक्तियों के बीच के सामाजिक अनुबंध से नहीं, बल्कि एक निश्चित ‘राष्ट्रीय आत्मा’ या ‘लोकाचार’ के साथ पैदा होता है.
- एकात्म मानववाद के मुताबिक, राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है, जिसे ‘चिति’ कहा गया है.
- एकात्म मानववाद के मुताबिक, समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास और उन्नयन करने से ही समाज का उत्थान होगा.
दीनदयाल उपाध्याय ने ‘एकात्म मानववाद’ के विचार दर्शन में प्रस्तुत किया । एकात्म मानववाद राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली आर्थिक क्रियायें हैं तथा जहां व्यक्ति दोनों का केन्द्र बिन्दु है। सिद्धांत बन सके और न ही ये स्थायी सत्यों से जुड़ पाये । निश्कर्षतः इसे पारिस्थितिक विलगाव पर आधारित सिद्धांत कहना उचित होगा।

एकात्म मानववाद मानव जीवन के सम्पूर्ण सृष्टि सम्बन्ध का दर्शन है। एकात्म मानववाद एक ऐसी धारणा है, जो सर्पिलाकार मण्डलाकृति द्वारा स्पष्ट की जा सकती है, जिसके केन्द्र में व्यक्ति, व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक घेरा परिवार, परिवार से जुड़ा हुआ घेरा समाज, जाति फिर राष्ट्र, विश्व और फिर अनंत ब्रह्माण्ड को अपने में समाविष्ट किये है। इस अखण्ड मण्डलाकार आकृति में एक घटक में से दूसरे,फिर दूसरे से तीसरे का विकास होता जाता है। सभी एक दूसरे से जुड़कर अपना अस्तित्व साधते हुए एक-दूसरे के पूरक एवं स्वाभाविक सहयोगी हैं। इनमें कोई संघर्ष नहीं है। एकात्म मानववाद में मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं और सृजित कानूनों के अनुरुप राजनीतिक कारवाई हेतु एक वैकल्पिक सन्दर्भ दिया गया है।
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय मानव को विभाजित करके देखने के पक्षधर नहीं थे। वे मानव-मात्र का हर उस दृष्टि से मूल्यांकन की बात करते हैं, जो उसके सम्पूर्ण जीवन काल में छोटी अथवा बड़ी जरुरत के रुप में सम्बन्ध रखता है। विश्व के इतिहास में ‘मानव-मात्र‘ के लिए अगर किसी एक विचार दर्शन ने समग्रता में चिंतन प्रस्तुत किया है तो वो ‘एकात्म मानववाद दर्शन‘ है। उनके अनुसार व्यक्ति शरीर में बुद्धि व आत्मा का एक समुच्चय है। अतः मानव के सन्दर्भ में इन चारों को विभाजित करके नहीं देखा जा सकता है, में परस्पर अंर्तसम्बन्ध हैं। एकात्म मानववाद उनके चिन्तन की एक ऐसी मौलिकता है, जो भारतीय इतिहास, परम्परा, राजनीति और भारतीय अर्थनीति के समावेशी धरातल पर स्थित है।
एकात्म मानववाद मानव में संवेदनशीलता की पुर्नस्थापना का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। इसलिए मानववाद जहाँ मानव को सम्पूर्ण सत्ता के केन्द्र में रखता है तो वहीं एकात्म मानववाद मानव मात्र की तात्विक एकता का सिद्धान्त है जो मानव के समग्र विकास का आधार है। उपाध्याय जी का मानना था कि ‘‘भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य और दर्शन सब भारतीय संस्कृति है जो राष्ट्रवाद का आधार है। इस संस्कृति में निष्ठा रखे तभी भारत एकात्म होगा।
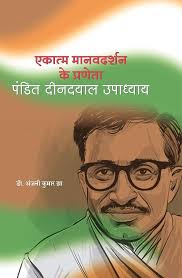
भारत में नैतिकता को सिद्धान्तों के अनुसार बदला जाता है, तब हमें संस्कृति और सभ्यता प्राप्त होते हैं। उपाध्याय जी का मानना है कि ‘‘शिक्षा और संस्कार से ही समाज के जीवन मूल्य बनते और सुदृढ़ होते हैं।‘‘ भारत में हमने अपने समक्ष मानव के समग्र विकास के लिए शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी विविध कामनाओं, इच्छाओं तथा एकताओं की सन्तुष्टि और उसके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से व्यक्ति के सामने कर्तव्य रूप में भारतीय संस्कृति में चतुर्विध पुरूषार्थ- धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की कल्पना की है। पुरूषार्थ का अर्थ उन कर्मों से है जिनसे पुरूषत्व सार्थक है। पुरूषार्थ की कामना मनुष्य में स्वाभाविक होती है और उनके पालन से उसको आनन्द प्राप्त होता है।
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भारत के सबसे तेजस्वी, तपस्वी एवं यशस्वी चिन्तक रहे हैं। उनके चिन्तन के मूल में लोकमंगल और राष्ट्र का कल्याण समाहित है। उन्होंने राष्ट्र को धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का सनातन पुंज बताते हुये राजनीति की नयी व्याख्या की। वह गांधी जी, तिलक और सुभाष की परम्परा के वाहक थे। वह दलगत एवं सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर वास्तव में एक ऐसे राजनीतिक दर्शन को विकसित करना चाहते थे, जो भारत की प्रकृति एवं परम्परा के अनुकूल हो और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने में समर्थ हो। अपनी व्याख्या को उन्होंने ‘‘एकात्म मानववाद‘‘ का नाम दिया।
दीनदयाल जी का जन्म 25 सितम्बर 1916 को निम्न मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। दीनदयाल जी की भारतीय लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। उनका मानना था कि लोकतंत्र भारत को पश्चिम की देय नहीं है। भारत की राज्यवधारणा स्वाभाविक रूप से लोकतन्त्रवादी रही है। वे लिखते हैं- ‘‘वैदिक सभा और समिति का गठन जनतंत्रीय आधार पर ही होता था तथा मध्यकालीन अनेक गणराज्य पूर्णतः जनतंत्रीय थे।‘‘
भारतीय दर्शन परम्परा प्राचीन काल से ही संघर्ष और द्वन्द की अपेक्षा समरसता को महत्व देती है। जिससे मानव का सम्पूर्ण विकास हो सके। यह व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही विकसित कर रखी थी। आवश्यकता उसे पुनः लोगों के सामने लाने की है। दीनदयाल जी ने वही कार्य किया जिसे वे एकात्म मानववाद के माध्यम से व्यक्त करते हैं। एकात्म मानववाद मानव जीवन में सामंजस्य स्थापित करके जीवन की समग्र सम्पन्नता एवं भव्यता के मार्ग को दिखाने वाला दर्शन है।
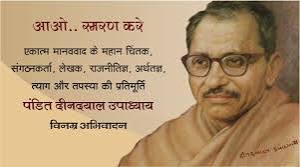
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि भारतवर्ष विश्व में सर्वप्रथम रहेगा, तो अपने सांस्कृतिक संस्कारो के कारण। उनके द्वारा स्थापित एकात्म मानववाद की परिभाषा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्यादा सामयिक है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा ये चारों अंग ठीक रहेगें तभी मनुष्य को चरम सुख और वैभव की प्राप्ति हो सकती हैं।आज भी उनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन शिक्षा की दृष्टि से प्रासंगिक प्रतीत होता है। आज आवश्यकता है कि सरकारें भी दीनदयाल उपाध्याय के इस दर्शन के अनुसार कार्य करें ।(विभूति फीचर्स)