(शिवशरण त्रिपाठी-विनायक फीचर्स)
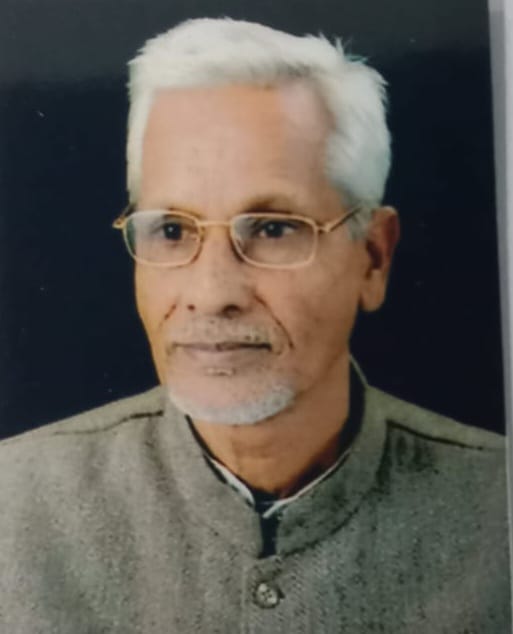
भारत का लोकतंत्र तीन स्तम्भों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर टिका है। संविधान में तीनों स्तम्भों के अधिकारों, कर्तव्यों की व्याख्या के साथ लक्ष्मण रेखा भी खींची गई है।
इसे दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि आये दिन विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बनती है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इसके लिये क्या स्वयं संविधान जिम्मेदार है अथवा स्वयं दोनों संवैधानिक संस्थायें? जो भी हो ऐसे हालात के लिये दोनो ही संवैधानिक संस्थायें जिम्मेदार रही हैं। ऐसे अनेक अवसर आये है जब विधायिका ने न्यायपालिका और न्यायपालिका ने विधायिका के अधिकारों का हनन करने में लक्ष्मण रेखा का उल्लघंन किया है। संविधान के तीनों स्तम्भ एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान व रक्षा करें यही भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिये अनिवार्य है। यदि ऐसा न हुआ तो आपसी टकराव तो बढ़ेगा ही लोकतंत्र मजाक बनकर रह जायेगा।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ ने न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिये समय सीमा निर्धारित किये जाने को लेकर न केवल सवाल उठाया वरन् उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुये यहां तक कह डाला कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों पर परमाणु मिसाइल नहीं दाग सकता।
उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनायेगें, जो कार्यपालिका के कार्य करेगें, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेगें और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून इन पर लागू नहीं होता है।
उपराष्ट्रपति ने लोगों को याद दिलाया कि भारत के राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव की शपथ लेते हैं। मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसद और न्यायाधीश सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा, हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें। और वह भी किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145 (3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। इसके लिए पांच या उससे अधिक न्यायाधीश होने चाहिए। उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए कहा कि जब सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, तो सरकार संसद के प्रति और चुनावों में जनता के प्रति जवाबदेह होती है।
क्या है अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके तहत कोर्ट किसी भी मामले में पूर्ण न्याय दिलाने के मकसद से ऐसा फैसला या आदेश दे सकता है, जो पूरे भारत में लागू हो, लेकिन यह आदेश
कैसे लागू होगा, यह संसद की ओर से बनाए गए कानून के जरिए तय होता है। अगर संसद ने अभी तक कोई नियम नहीं बनाया है, तो यह राष्ट्रपति को तय करना होता है कि कोर्ट की ओर से दिया गया आदेश या फैसला कैसे लागू किया जाए। इसके अलावा, अनुच्छेद के दूसरे हिस्से के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अपने सामने बुला सकता है, जरूरी दस्तावेज मांग सकता है।
अगर कोई इसकी अवमानना करता है, तो कोर्ट को इसकी जांच करके उसे सजा देने की शक्तियां भी हासिल है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को खास तरह के अधिकार देते है, जिसमें जब कानून का कोई उपाय काम नहीं करता तो कोर्ट उस मामले में पूर्ण न्याय दिलाने के मकसद के हिसाब से खुद अपने विवेक पर आगे बढ़कर फैसला ले सकता है।
इसी क्रम में उपराष्ट्रपति ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायमूर्ति के आवास से कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदगी से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज न किए जाने पर सवाल उठाया। धनखड़ ने कहा कहा कि अगर यह घटना उसके (आम आदमी के) घर पर हुई होती, तो इसकी (प्राथमिकी दर्ज किए जाने की) गति इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट सरीखी होती लेकिन इस मामले में तो यह बैलगाड़ी जैसी भी नहीं है।
उपराष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका पर उठाये गये कई सवाल उचित है तो कई अनुसचित भी। ठीक है न्यायपालिका को राष्ट्रपति को सीधे आदेश देने की बजाय सुझाव देना चाहिये था और तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्यपाल को भेजे गये दर्जन के करीब विधेयकों को राष्ट्रपति के पास न भेजे जाने पर सीधे निर्णय लेने की बजाय राज्यपाल से पूछा जाना चाहिये था कि आखिर उन्होने किन कारणों से एक लम्बे अर्से से विधेयकों को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिये भेजने की बजाय अपने पास रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा न करके सीधे निर्णय ही नहीं सुना दिया वरन् एक प्रकार से राष्ट्रपति की आलोचना भी कर डाली। हालांकि न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद इस सवाल का जवाब राज्यपाल को देना ही चाहिये कि आखिर उन्होने तमिलनाडु सरकार के विधेयकों को लम्बे समय से किन कारणों से रोक रखा था? राज्यपाल के चुप्पी साधने से साफ है कि उन्होने अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाने के बाद राष्ट्रपति को कम से कम राज्यपाल से सवाल तो पूछा ही जाना चाहिये था कि आखिर उन्होने क्यों और किस मंशा से विधेयकों को इतने लम्बे अर्से से अपने पास रोक रखा था। जहां तक दिल्ली के हाईकोर्ट के एक जज के घर में ही लाखों की नकदी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई विधिक कार्यवाही न करने पर सवाल उठाया गया वो उचित ही है।

क्या हाईकोर्ट का जज कानून से ऊपर है? अनेक अवसरों पर न्यायपालिका का पक्षपात भी सामने आता रहा है। जिस पर जनता में तीखी प्रतिक्रिया भी होती रही है। चाहे राम जन्म भूमि का मामला रहा हो, चाहे देश में आपातकाल लागू होने का, चाहे किसान आंदोलन में किसानों द्वारा लम्बे समय तक सड़कों पर आवागमन रोकने का और अब चाहे वक्फ कानून पर किन्तु परन्तु लगाये जाने का, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों व रूख से यही सिद्ध होता है कि वो कानून की समीक्षा करने के अपने अधिकार की आड़ में अपनी सीमायें लांघने में संकोच नहीं करता। वो जनहित के मामलों को जनमत के नजरिये से वरीयता देने की बजाय कानूनी दांव पेंच में फंसाने का जो खेल खेलता है उससे यही संकेत/ संदेश जाता है कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष नहीं रह गया है।
अतीत में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी लिये हैं। ऐसे में कहीं बेहतर होगा कि वो उसी मार्ग पर चले तो उसकी साख कायम रहेगी और राष्ट्र का भी कल्याण होगा। (विनायक फीचर्स)